UPTET Bal Vikas Evam Shiksha Shastra Bhasha Aur Vichar Study Material : आज की पोस्ट UPTET and CTET Bal Vikas Evam Shiksha Shastra Books and Notes Chapter 8 भाषा और विचार Study Material in Hindi साथ में Free PDF Download करने जा रहे है |
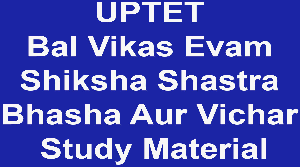
भाषा और विचार | UPTET Bal Vikas Evam Shiksha Shastra Book Chapter 8 in PDF
‘स्वीट’ (Siveet)के अनुसार, ”भाषा, ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हरलॉक (Hurlock) के अनुसार, ”भाषा में सम्प्रेषण (विचारों का आदान-प्रदान के वे सभी साधन आते हैं, जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। लिखना, पढ़ना बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव-भाव संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि भाषा में ही सम्मिलित हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है। यदि भाषा का विकास न हो तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास जिस सामान्य ढंग से होता है उस ढंग से नहीं होगा। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आ जाती है; अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है।
भाषा विकास का महत्व Importance of Language Development
भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है तथ है व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होत है। इसका महत्व निम्नलिखित है
(a) सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व (Importance of Language in Socies Relations) : भाषा के माध्यम से बालक अपनी बातों को दूसरे से कह सकता है तथ दूसरों की बात समझ भी सकता है तथा वाणी द्वारा वह सामाजिक मूल्यों, नियमों और आदर्शों आदि को सीखता है तथा समाज में समायोजन करने में सफल होता है। – एलिस के अनुसार, “भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अप समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है
(b) आत्म-मूल्यांकन में महत्व (Importance in Self Evaluation) : बालक ज ( अपने परिवार में होता है या अपने खेल के समूह में होता है अथवा अन्य किसी समूअ में होता है, उस समय दूसरे लोग उसके संबंध में क्या बोलते हैं और किस प्रकार (S मुखात्मक और शारीरिक अभिव्यक्ति करते हैं। इससे एक बालक सरलता से यह ज अ सकता है कि लोग उससे और उसकी वाणी से कितना प्रभावित हुए हैं।
(शैक्षिक उपलब्धि में महत्व (Importance in Academic Achievement): बाल अ को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसका शब्द-भण्डार कितना है, इन सभी बातो अ उसकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्रभावित होती हैं। जिनका शब्द-भण्डार बड़ा होता है उस वाक्य विन्यास तथा भाषा प्रस्तुतीकरण अच्छा होता है।
(d) नेतृत्व के विकास में सहायक भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समूह का नेता बन सकता है। वह अपनी बात दूसरों को समझा सकता है तथा दूसरों की बात को सुन सकता है। विचारों को जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर लेते हैं, उनकी वाणी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः नेतृत्व गुणों के विकास में भाषा सहयोग प्रदान करती है।
() व्यक्ति विकास में सहायक भाषा व्यक्ति विकास की आधारशिला है, जो बालक अपने विचारों का प्रकटीकरण सीमित, सन्तुलित तथा प्रभावशाली भाषा में करते हैं, वे जीवन में विकास की ओर बढ़ते हैं तथा उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है।
() सामाजिक मूल्यांकन में महत्व (Importance in Social Evaluation): जिस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में बालक दूसरों की वाणी सुनकर अपना या आत्म-मूल्यांकन करता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में एक बालक क्या बोलता है या क्या उसकी वाणी सम्बन्धित अभिव्यक्ति है, इस आधार पर उस बालक का मूल्यांकन समाज के अन्य व्यक्ति करते हैं।
भाषा विकास के सिद्धांत Principle of Language Development
भाषा विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं-
(a) स्वर यंत्र की परिपक्वता (Maturation of Larynx): भाषा का विकास शरीर के अंग की परिपक्वता जैसे—स्वर यंत्र, जीभ, गला और फेफड़ा इत्यादि पर निर्भर करता है। यह सभी अंग जब तक एक विशेष परिपक्वता स्तर पर नहीं पहुँचते हैं तब तक भाषा का सामान्य विकास संभव नहीं है। इन सभी अंगों के अतिरिक्त भाषा का विकास होंठ, दाँत, तालु और नाक के विकास पर भी निर्भर करता है।
इन अंगों की परिपक्वता के अतिरिक्त वातावरण संबंधी कारक भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा के विकास में वातावरण संबंधी कारकों में अनुकरण के अवसर एक महत्वपूर्ण कारक हैं।
L) अनुबंधन (Conditioning) : अधिगम सिद्धान्तवादियों ने बालक में भाषा के विकास को उद्दीपक अनुक्रिया (S-R) के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया है। इस दिशा में स्किनर (Skinner) का प्रयास अति सराहनीय है। स्किनर ने पुनर्बलन Reinforcement) के आधार पर भाषा के विकास को समझाया। स्किनर का विचार है के अन्य व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का विकास भी ‘आपरेन्ट अनुबंधन’ (Operant Conditioning) पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि-संयोजन (Sound Combination)के चयनात्मक पुनर्बलन |Selective Reinforcement) पर निर्भर करता है। स्किनर के अनुसार बालक स्वतः अनायास या अनुकरण के आधार पर बोलते हैं।
उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी बालक शब्दों का प्रधिगम करता है। अतः स्किनर के अनसार बालक का शब्दों को सीखना आपरेन्ट अनुबंधन से अधिक सम्बन्धित है।
कोमास्की का सिद्धांत (Chomsky’s Theory):कोमास्की (Chomsky)का विचार कि बालक का शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारितअवश्य है परन्तु अनुकरण और पनर्बलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को भली-भाँति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमास्की ने अपने सिद्धांत को निम्नलिखित मॉडल चित्र के द्वारा समझाया हैLinguistic Data T LAD The Ability to Understand & (Input) (Processing) Produce Sentence (Output)
“उपर्युक्त मॉडल के अनुसार बालक जो कुछ भी सुनता है उसे Language Acquisition Device) के द्वारा समझता है तथा उसे पुनरोत्पादित कर सकता है तथा नये शब्द भी बोल सकता है।
(d) सामाजिक अधिगम सिद्धांत (Social Learning Theory) : इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बन्डुरा (Bandura) का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है, वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण .और अनुकरण पर आधारित होता है। इस प्रकार का सीखना पुनर्बलन के साथ भी हो , सकता है और पुनर्बलन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है।
इन सिद्धांतवादियों का कहना है कि बिना किसी मॉडल के बच्चे शब्दों और भाष – की संरचना को नहीं सीख सकते हैं। बालक जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें रहने । वाले अन्य व्यक्ति जो भाषा और शब्द बोलते हैं, वह बच्चा सुनता रहता है। कई बार कि वह शब्दों का तुरंत अनुकरण नहीं कर पाते हैं। फिर भी वे शब्दों और भाषा के बारे में। कुछ सूचना अवश्य ग्रहण करते हैं।
भाषा-विकास की अवस्थाएँ Stages of Speech Development
बालकों में भाषा-विकास की कई अवस्थाएँ हैं, जो इस प्रकार है-
A. बोलने की तैयारी
क्रन्दन (Crying) शिशु के जन्म से ही क्रन्दन प्रारम्भ हो जाता है, जो उसर्व वा भाषा का प्रारम्भिक रूप है। यदि बालक सामान्य रूप से रोता है तो रोने से उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। साथ ही उसकी माँसपेशियों का अभ्यास भी हो जात । है। इस अभ्यास से उसकी माँसपेशियों की वृद्धि होती है और माँसपेशियों का समन्वय (Ordination) बढ़ता है। रोने से उनको अच्छी नींद आती है एवं उनकी भूख बढ़ती है 3 रोने से बच्चों का संवेगात्मक तनाव भी दूर होता है, परन्तु आवश्यकता से अधिध रोना बालक के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से हानिकारक होता है।
- वा तक चलता है। बबलाने से बालकों के स्वर-यन्त्र की परिपक्वता को बल मिलता बालक आय बढ़ने के साथ अधिक से अधिक ध्वनियाँ बोलने लगता है। बबलाने में वा स्वरों को पहले और व्यंजनों को उनके साथ मिलाकर दुहराता है।
हाव भाव (Gestures): बालकों द्वारा हाव-भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप किया जाता है। बच्चों के हाव-भाव की उत्पत्ति बबलाने के साथ साथ ही हो जाती बच्चा अपने हाव-भाव का प्रदर्शन, मुस्कुराकर, हाथ फैलाकर, अँगुली दिखाकर, मूक में करता है। अतः बच्चों के लिए हाव-भाव विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुगम मशन है, जो शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है।
वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ
(a) आकलन शक्ति (Comprehensive Power) : बालकों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं तथा हाव-भाव का अनुकरण कर लेता है, ‘आकलन शक्ति कहलाती है। हरलॉक के अनुसार, बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। प्रायः यह देखा गया है कि बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है, जिनमें शब्दों के साथ-साथ कुछ हाव-भाव भी जुड़े होते हैं।
(b) उच्चारण (Pronunciation): लगभग 1 वर्ष के बालकों में शब्दों के अनुसार उच्चारण की तत्परता (Readiness) एवं योग्यता आ जाती है। इस समय वह अनेक ऐसी सरल ध्वनियों को उच्चारित कर सकता है जिनका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया था। यह वह अनुकरण द्वारा सीखता है।
(c) शब्द-भण्डार (Vocabulary) : बालक के शब्द-भण्डार में वृद्धि उसके आयु में वृ द्धि के साथ-साथ होती है।
बालक का शब्द-भण्डार Vocabulary of Child
बालक का शब्द भण्डार
विशिष्ट शब्दावली का रूप शिष्टाचार से सम्बन्धित शब्द-भण्डार (Etiquette Vocabulary) गुप्त शब्द भण्डार (Secret Language) अशिष्ट शब्द भण्डार (Slang Vocabulary) धन से सम्बन्धित भण्डार (Money Vocabulary) रंगों से सम्बन्धित भण्डार (Colour Vocabulary) संख्याओं से सम्बन्धित भण्डार (Number Vocabulary) समय संबंधी शब्द (Time Vocabulary) atrafor (Sentence Formation) शुद्ध उच्चारण (Correct Pronunciation) साधारण शब्द भण्डार भाषा या वाणी शब्द (Speech Defects) शब्द-अर्थ से सम्बधित दोष वाक्य-निर्माण में दोष उच्चारण में दोष (Defects in Pronunciation)
> थॉमसन तथा लिपसिट के अनुसार,
10 शब्द 18 माह के बालक का शब्द भण्डार
272 शब्द 2 वर्ष
450 शब्द 2, वर्ष
1000 शब्द 3 वर्ष
1250 शब्द 37 वर्ष
1600 शब्द 4 वर्ष
1900 शब्द 4 वर्ष
2100 शब्द 5 वर्ष
50,000 शब्द छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द-भण्डार हाई स्कूल80,000 शब्द >
बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द-भण्डार अधिक होता है।
सामान्य भाषा या वाणी विकार Some Common Speech Defects
अधिकांशतः वाणी संबंधी विकार उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। उन बालकों की भाषा धीमी गति से व क्रमिक होता है। सामान्य भाषा में दोष निम्नलिखित प्रकार से होते हैं
(a) भ्रष्ट उच्चारण (Lisping) : सामान्य वाणी दोषों में मुख्यतः भ्रष्ट उच्चारण-दोष पाया जाता है। मुख्य रूप से जबड़ों, दाँतों और होंठों की रचना ठीक न होने के कारण : या परिवार के सदस्यों द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना या फिर शैशवावस्था में बच्चों द्वार । उच्चारित शब्द का माता-पिता द्वारा आनन्द लेना तथा भ्रष्ट उच्चारण को प्रोत्साहित करन = इत्यादि भ्रष्ट उच्चारण-दोष को बढ़ावा देता है।
(b) अस्पष्ट उच्चारण (Slurring) : बच्चे जब शब्दों को अस्पष्ट बोलते हैं तो इस 2 प्रकार का विकार भाषा विकार कहलाता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बच्च में अस्पष्ट उच्चारण करता है लेकिन आयु बढ़ने के साथ-साथ इस प्रकार का विकार स्वाद ही दूर हो जाता है।
(c) तुतलाना (Sluttering) : वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश बालकों में यह भाषा दोष 2 वर्ष की अवस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है। बालकों का समायोजन जैसे जैसे अच्छा होता है, उसका तुतलाना कम हो जाता है।
हकलाना (Stammering) : वैज्ञानिकों का मानना है कि हकलाने का कारण बालकों का भय और घबराहट है। इसके अतिरिक्त स्वरयन्त्र, गला, जीभ, फेफड़ों तहा होंठ सभी का सन्तुलन ठीक न होने पर बालकों में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ट्रेविस मतानुसार, हकलाने का कारण मस्तिष्क में श्रवण एवं वाक् केन्द्रों का विकृत हो जाना के
(e) तीव्र अस्पष्ट वाणी (Cluttering) : बच्चे की वाणी तीव्र अस्पष्ट होती है। इस बच्चे के बोलने की गति तीव्र हो जाती है और साथ साथ शब्द अस्पष्ट होते हैं। तीव्र और अस्पष्ट होने के कारण बोलने वाले की भाषा कहीं कहीं समझ में नहीं आती है।
भाषा और विचार कास को प्रभावित करने वाले कारक Factors Affecting Language Development,
भाषा-विकास में वैयक्तिक करनेवाले कारक निम्नलिखित हैं-
में वैयक्तिक भिन्नता पायी जाती है। भाषा-विकास को प्रभावित विभिन्न अंगों की परिपक्वता अ पता (Maturation) : जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के की परिपक्वता आवश्यक है। उसी प्रकार भाषा-विकास के लिए भी होंठ. साडे स्वरयंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है।
बदि (Intelligence) विभिन्न अध्ययन में यह देखा गया है कि जिन बच्चों की
उच्च होती है, उनका कम IQ वाले बालकों की अपेक्षा शब्द-भण्डार अधिक ना है। उच्च IQ वाले बालक शुद्ध और बड़े वाक्य भी बोलते हैं। अधिक बुद्धि वाले बालकों में शब्द-भण्डार एवं वाक्य-रचना की अधिक क्षमता और शुद्ध उच्चारण की क्षमता भी पायी जाती है।
(c) स्वास्थ्य (Health) : यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप 5 से दो वर्ष की आयु की अवधि तक तो उसके भाषा का विकास कमजोर स्वास्थ्य और 5 अभ्यास न कर सकने के कारण पिछड़ जाता है। बीमार बालक में भाषा बोलने के लिए (सीखने की प्रेरणा का अभाव भी पाया जाता है।
(d) यौन (Sex) : मैकनील का विचार है कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा-विकास ग में बालिकाओं से पीछे रहते हैं। लड़कियों का शब्द-भण्डार, वाक्य में शब्दों की संख्या, – शब्द-चयन और वाक्य-प्रयोग आदि में लड़कों से अच्छा होता है। लड़कियाँ लड़कों की जा अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं।
(e) सामाजिक अधिगम के अवसर (Social Learning Opportunity) : बालक को – भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं या जिन परिवार म बच्चे अधिक होते हैं, उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि पूसर बच्चे को सुनकर उनका अनुकरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं।
जब परिवार में बच्चे न हों तो माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बालक को पड़ोस क बच्चों के साथ खेलने का अवसर दें जिससे कि बच्चा दूसरे बच्चों का अनुकरण करके भाषा जल्दी सीख जाय।
दशन (Guidance) : बालकों की भाषा के विकास के लिए माता-पिता और का आदि का निर्देशन भी आवश्यक है। बालक की भाषा उतनी ही अच्छी विकसित जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किये जाते है। | (Motivation): अभिभावकों को चाहिए कि वे बालकों को हमेशा सीखने करते रहें। अभिभावक को बालकों के रोने पर वह चीज उपलब्ध नहीं जसक लिए वह रो रहा है तथा बालक यदि संकेत और हाव-भाव क । ता भी उपलब्ध न कराएँ, क्योंकि इस प्रकार बालक शब्दों को अध्यापकों आदि का निर्देशन भ क) (g) प्रेरणा (Motivation) : आ के लिए प्रेरित करते रहे। अ किराना चाहिए जिसके लिए प्रयोग में कोई चीज माँगे ता सीखने के लिए प्रेरित होंगे।
(h) सामाजिक आर्थिक स्थिति (Socio-Economic Status) : ऐसे बालक जिसक सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होता है। उच्च सामाजिक स्तर वाले बालक पहले बोलना अधिक बोलना व अच्छा बोलना अपेक्षाकृत शीघ्र सीखते हैं।
(i) शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना (Physical Health and Body Structures जो बच्चे स्वस्थ, निरोगी होते हैं उनका भावात्मक विकास शीघ्र होता है। शारीरिक रचन भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। शरीर रचना या शारीरिक रचना से अभिप्राय स्वरयंत्र, तालु, जीभ, दाँतों आदि की बनावट से है, क्योंकि ये अंश बोलने की क्रिय में भाग लेता है। ____6) व्यक्तिगत विभिन्नताएँ (Individual Differences) जो बच्चे उत्साही होते। उनमें शान्त प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा शीघ्र विकसित होती है।
(K) कई भाषाओं का प्रयोग (Bilingualism): छोटे बच्चों के माता-पिता की भाष यदि अलग-अलग हो, तो बच्चे में भाषा का विकास अवरुद्ध होकर मन्द गति से होता है |
() पारिवारिक संबंध (Family Relationship) जिन बच्चों के पारिवारिक संबं अच्छे नहीं होते हैं उनमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आका भी भाषा विकार को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता-पिता बालकों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। फलस्वरूप उनमें भाषा का विकार शीघ्र होता है। परन्तु यदि माता-पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चों में भाषा का विकास दे से होता है।
बालकों की भाषा में सुधार के सुझाव Suggestions for Improving Children’s Speech
बालकों की भाषा में सुधार के सुझाव निम्नलिखित हैं-
(a) बालकों को उसकी उम्र के बराबर के बच्चों में अक्सर रखना चाहिए और बच्च को हमउम्र बच्चों से बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए।
(b) बच्चों की भाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर उनमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन् करनी चाहिए।
4) बच्चों की त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण या विकारयुक्त वाणी की आलोचना नहीं कर चाहिए, ताकि बच्चों में भाषा बोलने के प्रति आत्मविश्वास जागृत हो।
(d) बालकों को कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। (e) जिन बालकों में भाषा-दोष हो उनका उपहास नहीं करना चाहिए।
(6) बालकों में अच्छी वाणी के विकास के लिए उनके सामने अच्छी भाषा का प्रय करना चाहिए ताकि बच्चे वाक्यों का अनुसरण करें। भाषा सीखने के साधन (a) अनुकरण (Imitation) ___(b) खेल (Play) (c) कहानी सुनना (Listening of Stories) (d) वार्तालाप तथा बातचीत (Talking) (e) प्रश्नोत्तर (Question -Answer)
विचार Thought
भाषा-सम्प्रेषण के माध्यम कौशल आदि सीखाने का प्रयास क पण के माध्यम से बालक नये भाव, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार तथा ल सीखाने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब शिक्षक और बालक क लक के उस भाषा का ज्ञान हो। सम्प्रेषण को समझने के बाद बालक अपनी स न अनक्रिया विचार के रूप में व्यक्त करता है।
विचार के प्रकार
शाब्दिक विचार मौखिक विचार
दृष्टि-विचार → मौखिक दृष्टि विचार
लिखित विचार
अशाब्दिक विचार शारीरिक भाषा कूट भाषा
परीक्षोपयोगी तथ्य
> भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुँचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं एवं
भावों को ग्रहण करता है।
> मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के चरणों की व्याख्या मोटे तौर पर दो भागों में बाँटकर किया है-
बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। बोलने की तैयारी में क्रन्दन, बबलाना एवं हाव-भाव शामिल है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द-भण्डार इत्यादि शामिल है।
शिक्षा मनोवैज्ञानिकों तथा विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा विकास एक खास क्रम में होता है। इस क्रम का पहला चरण ध्वनि की पहचान तथा अंतिम चरण भाषा विकास की पूर्णावस्था है।
बालकों के भाषा विकास कई कारणों से प्रभावित होते हैं जिनमें बुद्धि, स्वास्थ्य, बान-भिन्नता, सामाजिक-आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, बहुजन्म, एक से अधिक भाषा-उपयोग, साथियों के साथ संबंध तथा माता-पिता द्वारा प्रेरणा प्रधान है।
बालका में दो तरह के शब्दावली विकसित होते हैं सामान्य शब्दावली तथा विशिष्ट शब्दावली।
भाषा-विकास में घर पर माता-पिता द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा तथा स्कूल में ससका द्वारा दी गई अौपचारिक शिक्षा का काफी महत्व होता है।
Download UPTET Bal Vikas Evam Shiksha Shastra Book Chapter 8 भाषा और विचार in Hindi PDF
| बाल भाषा और विचार in PDF | Download |